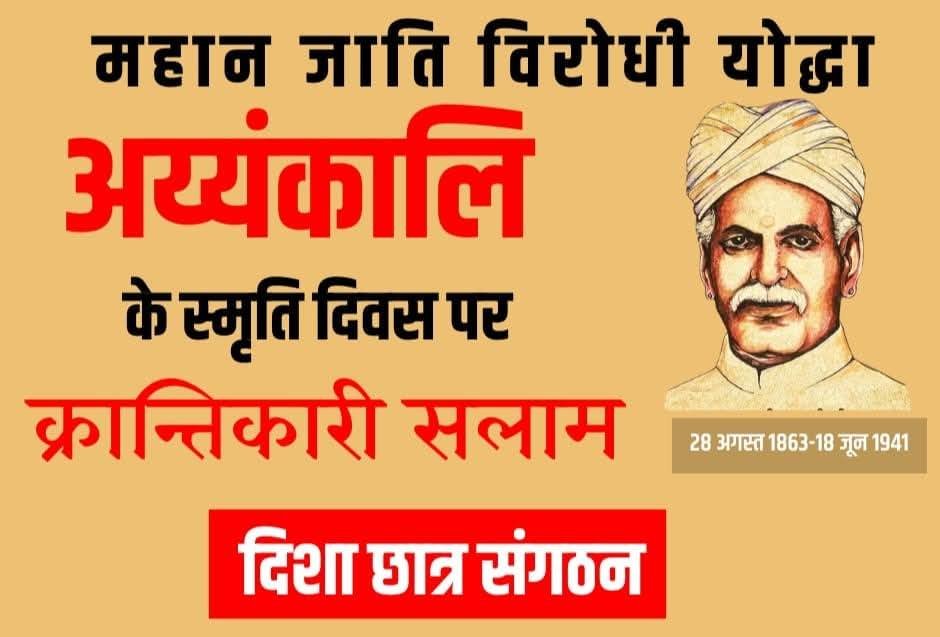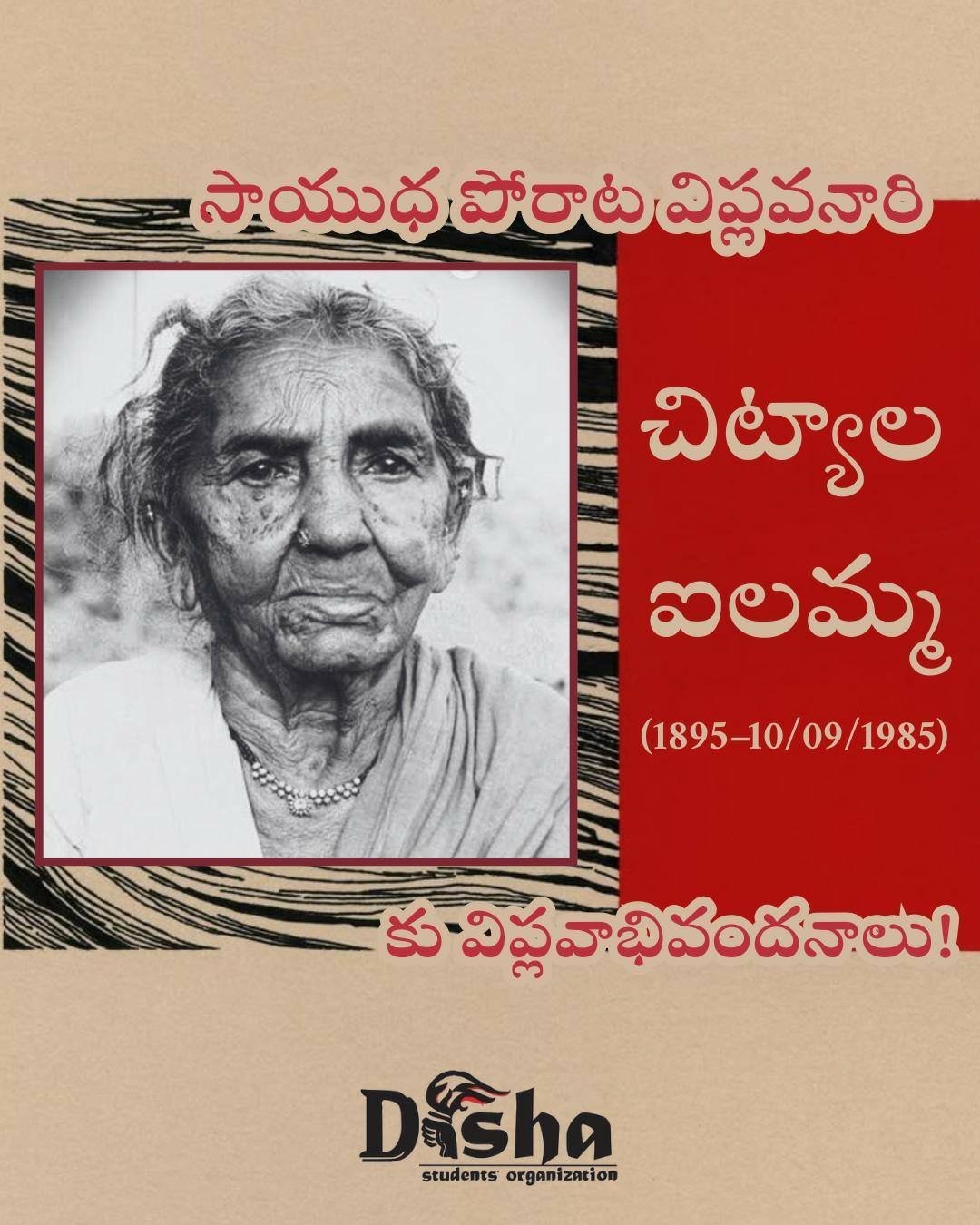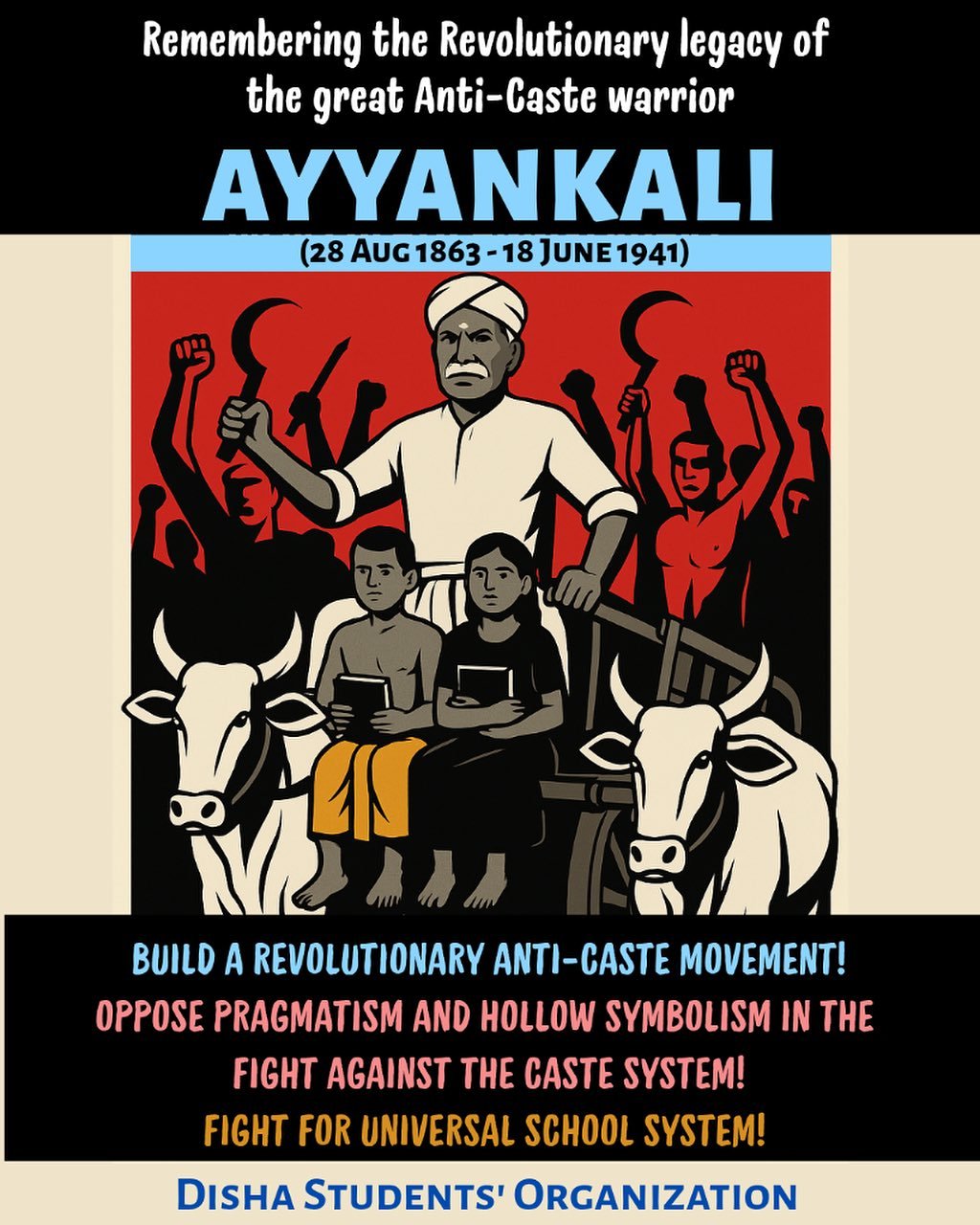महान जाति-विरोधी योद्धा अय्यंकालि के स्मृति दिवस (18 जून) के अवसर पर
अय्यंकालि की विरासत को याद करो! क्रान्तिकारी जाति-उन्मूलन आन्दोलन को आगे बढ़ाओ!
साथियो!
आपमें से शायद कुछ ने ही महान जाति-विरोधी योद्धा अय्यंकालि का नाम सुना हो। इसकी वजह समझी जा सकती है। अय्यंकालि उन जाति-विरोधी योद्धाओं में से थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादियों और उनकी सत्ता से समानता का हक़ हासिल करने के लिए एक जुझारू लड़ाई लड़ी और कामयाब हुए। उन्होंने सरकार का इन्तज़ार नहीं किया जो बिरले ही ब्राह्मणवादियों और उच्च जाति के सामन्तों के विरुद्ध जाती थी, क्योंकि ये सामन्ती ब्राह्मणवादी शक्तियों तो शुरू से अन्त तक ब्रिटिश सत्ता के चाटुकार और समर्थक रहीं। अय्यंकालि ने सुधारों के लिए प्रार्थनाएं और अर्जियाँ नहीं दीं, बल्कि सड़क पर उतर कर ब्राह्मणवादियों की सत्ता को खुली चुनौती दी और उन्हें परास्त भी किया। अय्यंकालि ने सिद्ध किया कि दमित और उत्पीडि़त आबादी न सिर्फ लड़ सकती है, बल्कि जीत भी सकती है। अय्यंकालि का संघर्ष आज के जाति-उन्मूलन आन्दोलन के लिए बेहद प्रासंगिक है। आज अय्यंकालि के संघर्ष को याद करना जाति-उन्मूलन के आन्दोलन को सुधारवाद व व्यवहारवाद के गोल चक्कर से निकालने के लिए ज़रूरी है।
कौन थे अय्यंकालि?
अय्यंकालि का जन्म 28 अगस्त 1863 को ब्रिटिश भारत के दक्षिण में त्रावणकोर की रियासत में तिरुवनन्तपुरम जिला के वेंगनूर में हुआ था। उनका जन्म केरल की सर्वाधिक दमित व उत्पीडि़त दलित जातियों में से एक पुलयार जाति में हुआ था। त्रावणकोर में पुलयार लोगों को ब्राह्मणवादी पदानुक्रम में सबसे नीचे का स्थान दिया गया था। उन्हें नायर जाति के ज़मींदारों से लेकर ब्राह्मणों तक के अपमानजनक और बर्बर किस्म के दमन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति ने अय्यंकालि के दिल में बग़ावत की आग को जलाया। शुरुआत में वे अपने अन्य पुलयार दोस्तों के साथ मिलकर काम के बाद ऐसे गीतों और नृत्यों का सृजन करने लगे जो कि इस स्थिति के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। इसके कारण कई युवा दलित उनसे जुड़ने लगे। अय्यंकालि शुरू से ही समझते थे कि उच्च जातियों द्वारा दलितों के दमन और उनके ख़िलाफ की जाने वाली हिंसा के प्रश्न पर अंग्रेज़ सरकार कुछ नहीं करने वाली है। इसलिए इस दमन और हिंसा का जवाब उन्होंने खुद सड़कों पर देने का रास्ता अपनाया। उनके इर्द-गिर्द एकत्र युवाओं का एक समूह अस्तित्व में आने लगा और यह समूह हर हमले का जवाब ब्राह्मणवादियों को सड़कों पर देने लगा। यह हिंसा वास्तव में आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा थी। लेकिन इस प्रकार के जवाबी हमलों ने ब्राह्मणवादी शक्तियों को सकते में ला दिया। अय्यंकालि के इस रास्ते के चलते दलित आम मेहनतकश आबादी उन्हें चाहने लगी और उन्हें कई प्रकार की उपाधियाँ देने लगी जैसे कि उर्पिल्लई और मूथपिल्ला।
अय्यंकालि कई प्रकार के धार्मिक सुधारकों से प्रभावित हुए जिनमें अय्यावु स्वामिकल और नारायण गुरू प्रमुख थे। ये दोनों ही हिन्दू धर्म के भीतर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। मानवतावाद इनके धार्मिक दर्शन का आधार था। यही कारण था कि नारायण गुरू ने अपनी एक रचना में हिन्दू देवताओं के अलावा ईसा और मुहम्मद को भी ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और कहा कि ये सभी एक ही मानवतावादी विचार का समर्थन करते हैं और ये विचार जाति प्रथा के ख़िलाफ़ हैं। अय्यंकालि दार्शनिक तौर पर धार्मिक सुधार आन्दोलन से आगे नहीं गये। इस रूप में वे एक सामाजिक व राजनीतिक क्रान्तिकारी तो थे, लेकिन वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोण तक नहीं पहुँच पाये थे। इसका एक कारण यह था कि अय्यंकालि निरक्षर थे और उनके पास विज्ञान का कोई शिक्षण नहीं था। साथ ही, उनके समय के केरल के समाज में तर्कवाद और भौतिकवाद को स्थापित करने की लड़ाई अभी अपने भ्रूण रूप में ही थी। लेकिन किसी भी जन नेता या संगठन के प्रगतिशील होने का पैमाना यह नहीं कि वह भौतिकवादी था या नहीं, बल्कि यह होता है कि वह अपने दौर के दमन और शोषण के ख़िलाफ़ क्रान्तिकारी तरीक़े से लड़ता है या नहीं। यानी वह दमनकारी सत्ता के विरोधी नज़रिये को अपनाता है या नहीं। यदि कोई भौतिकवाद को मानकर भी राजनीतिक तौर पर सुधारवाद और व्यवहारवाद पर चले, तो ऐतिहासिक तौर पर वह क्रान्तिकारी प्रगतिशील नहीं माना जा सकता है। अगर यह बात न समझी जाय तो पूरे मानव इतिहास में वैज्ञानिक भौतिकवादियों के अलावा कोई प्रगतिशील ही नहीं रह जायेगा: न स्पार्टकस, न मौर्य काल में हुए पहले शूद्रों व दलितों के विद्रोह के नेता, न बिरसा मुण्डा, न चीनी ताइपिंग किसान विद्रोह के नेता, और न ही हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाली शुरुआती क्रान्तिकारी धाराएँ जैसे कि ‘युगान्तर’ व ‘अनुशीलन’।
इसके बावजूद सबसे अहम बात यह है कि अय्यंकालि अपने संघर्ष के तौर-तरीकों में एक वैज्ञानिक और भौतिकवादी थे। वे किसी भी दमित व उत्पीडित आबादी के संघर्ष में बल की भूमिका को समझते थे। वे समझते थे कि लुटेरे और दमनकारी शासकों का सलाह व सुझाव देने से दिल नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उनका शासन ही मेहनतकश व दलित जनता की लूट और दमन पर टिका है। उन्हें संगठित होकर अपनी ताक़त के बल पर झुकाया जा सकता है। वे किसी ईश्वरीय शक्ति के भरोसे नहीं बैठे रहे, बल्कि उन्होंने दमन व उत्पीड़न के ख़िलाफ़ ख़ुद सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया। वे ब्रिटिश सरकार के भी भरोसे नहीं बैठे रहे, बल्कि संगठित जन के बल प्रयोग से ब्राह्मणवादी शक्तियों को झुकने पर मजबूर कर दिया।
अय्यंकालि का महत्व आज सबसे ज्यादा इसी बात के लिए है। आज भी सुधारवाद और व्यवहारवाद की सोच जाति-उन्मूलन के आन्दोलन पर हावी है। यह सोच इस आन्दोलन को कई दशकों से सरकार को अर्जियां देने, प्रार्थनाएं करने, इस या उस पूँजीवादी पार्टी की पूँछ पकड़कर चलने और अस्मितावाद की खोखली सोच से आगे नहीं जाने दे रही है। ऐसे में, जाति-अन्त के आन्दोलन को सही रूप में आगे ले जाने के लिए अय्यंकालि के आन्दोलन की विरासत बेहद अहम है। अफ़सोस की बात है कि अधिकांश मेहनतकश दलित भाई और बहन इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारत की पूँजीवादी सत्ता ने दलित आन्दोलन में सुधारवाद और व्यवहारवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार इसने ऐसे सभी जाति-विरोधी योद्धाओं की विरासत को जनता से छिपाया और दूर किया, जो कि जाति अन्त की लड़ाई में क्रान्तिकारी तरीक़े से सत्ता-विरोधी रास्ते को अपनाते थे।
अय्यंकालि ने क्या किया था?
अय्यंकालि ने खुले तौर पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए 1893 में एक ऐसा आन्दोलन शुरू किया, जिसने केरल के समाज की तस्वीर को बदल डाला। अय्यंकालि ने एक बैलगाड़ी ख़रीदी (जिसकी आज्ञा उस समय दलितों को नहीं थी), ऐसे कपड़े पहने जिनका अधिकार केवल उच्च जातियों को था, और एक सार्वजनिक सड़क के बीचों-बीच हाथ में एक हथियार लिए निकल पड़े। उस समय पुलयारों व अन्य दलितों को यह अधिकार नहीं हासिल था कि वे सार्वजनिक सड़कों पर चल सकें। उन्हें सड़कों के किनारे मिट्टी व कीचड़ में चलना पड़ता था। जब अय्यंकालि ने यह विद्रोह की कार्रवाई की तो ब्राह्मणों व अन्य उच्च जाति के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गयी। लेकिन अय्यंकालि के हाथों में हथियार देखकर किसी को भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। अय्यंकालि की इस कार्रवाई से पूरे त्रावणकोर रियासत के दलितों में एक लहर फैल गयी। जगह-जगह दलितों ने इसी प्रकार की बग़ावती कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू किया। इसकी वजह से कई जगहों पर दलितों व उच्च जातियों की सामन्ती शक्तियों की बीच सड़कों पर हिंस्र टकराव हुए। इनको चेलियार दंगों के नाम से जाना जाता है। दोनों ही पक्षों के लोग हताहत हुए। लेकिन इन विद्रोहों के कारण सन् 1900 तक यह स्थिति पैदा हो गयी कि केरल में दलित अधिकांश सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार हासिल कर चुके थे। यह अय्यंकालि का पहला बड़ा क्रान्तिकारी संघर्ष और विजय थी।
कुछ पुलयारों को ईसाई मिशनरी स्कूलों में शिक्षा का सीमित अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन शिक्षा पाने के लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना होता था। लेकिन अय्यंकालि का मानना था कि सभी सार्वजनिक स्कूलों में दलितों को बराबरी से शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने कहने के लिए 1907 में दलित बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाख़िले का अधिकार दिया, लेकिन स्थानीय अधिकारी आराम से यह अधिकार छीन लेते थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को यह पता नहीं था। लेकिन उसने कभी भी ऐसे ब्राह्मणवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे प्रमुख समर्थन आधार ब्राह्मणवादी सामन्ती शक्तियाँ ही थीं। अय्यंकालि ने 1907 में ही साधु जन प्रपालना परिषद् (गरीबों की सुरक्षा हेतु संगठन) बनाया था। पहले तो अय्यंकालि ने पुलयारों द्वारा संचालित स्कूलों को स्थापित करने के लिए आन्दोलन किया। लेकिन इसके बाद उनका आन्दोलन सरकार और ब्राह्मणवादी सामन्तों के विरुद्ध बन गया। इसका कारण यह था कि उन्होंने एक दलित बच्ची का दाख़िला एक सरकारी स्कूल में करवाने का प्रयास किया लेकिन इसके जवाब में ब्राह्मणवादियों ने दलितों पर हिंस्र हमले किये और ऊरुट्टमबलम में एक स्कूल को जला दिया। इसके जवाब में अय्यंकालि ने सभी खेतिहर मज़दूरों की एक हड़ताल संगठित की। इनमें से अधिकांश दलित थे। यह आधुनिक भारत में खेतिहर मज़दूरों की पहली हड़ताल थी। इस हड़ताल को अय्यंकालि ने तब तक जारी रखा जब तक कि सभी दलित बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना रोक-टोक दाखिले का अधिकार नहीं मिल गया। यह आधुनिक भारत के इतिहास में खेतिहर मज़दूरों की पहली हड़ताल थी। इस दौरान जब भी दलितों पर उच्च जाति के सामन्तों ने हमले किये तो अय्यांकालि के संगठन के नेतृत्व में दलितों ने भी जवाबी हमले किये। इस वजह से उच्च जाति सामन्तों को अब हमला करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता था और उनके हमले नगण्य हो गये। इस आन्दोलन ने जनता की क्रान्तिकारी पहलक़दमी को खोला और उन्हें स्वयं संगठित होकर सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन का रास्ता दिखलाया। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी।
अय्यंकालि ने पुलयार जाति की स्त्रियों के लिए ऊपरी शरीर को ढकने के अधिकार के लिए आन्दोलन में केन्द्रीय भूमिका निभाई। नादरों को यह अधिकार अपने आन्दोलन के कारण पहले ही मिल चुका था, लेकिन पुलयारों को यह अधिकार 1915 में जाकर हासिल हुआ। इस आन्दोलन में भी अय्यंकालि ने किसी प्रबुद्ध प्रशासक को अर्जियाँ देने या बुद्धिजीवियों के द्वारा सरकार को प्रार्थनाएँ और सलाहें पेश करने पर नहीं बल्कि जनता की संगठित पहलक़दमी पर भरोसा किया। इन सभी आन्दोलनों के ज़रिये अय्यंकालि ने दिखलाया कि समाज में दलितों को वास्तविक अधिकार रैडिकल जनसंघर्षों के बूते मिले। उनका पहला ज़ोर ही हमेशा जनता को रैडिकल संघर्षों के लिए संगठित करने के लिए होता था, जो कि सरकार के विरुद्ध होते थे। वे सरकार को प्रार्थना पत्र लिखने में कम भरोसा करते थे और मानते थे कि चीज़ें सरकार को लिखे गये आवेदन पत्रों से नहीं बदलतीं, क्योंकि सरकार दलितों व ग़रीबों के पक्ष में नहीं होती बल्कि शासक वर्ग की नुमाइन्दगी करती है। वे जानते थे कि इस सरकार के खिलाफ जुझारू जनसंघर्षों के बूते ही चीज़ों को बदला जा सकता है।
अय्यंकालि से आज का जाति-उन्मूलन आन्दोलन क्या सीख सकता है?
अय्यंकालि से आज का जाति-उन्मूलन आन्दोलन तीन चीज़ें सीख सकता है और उसी सीखना ही चाहिए। पहला, जनता की शक्ति और पहलक़दमी पर भरोसा और दूसरा, आवेदनबाज़ी, अर्जियाँ देने और प्रार्थना-पत्रों की बजाय रैडिकल सत्ता-विरोधी जनसंघर्षों से दलित मुक्ति का संघर्ष। अफ़सोस की बात है कि दलित मुक्ति के संघर्ष का बड़ा हिस्सा आज सुधारवाद, व्यवहारवाद और अस्मितावाद के दलदल में धँसा हुआ है। इस व्यवहारवाद के ही तार्किक परिणति के तौर पर आठवले, मायावती, पासवान, उदित राज और थिरुमावलवन जैसे लोग पैदा होते हैं, जो कि सवर्णवादी प्रतिक्रियावादी और पूँजीवादी शक्तियों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और दलित अस्मिता के नाम पर दलित मेहनतकश आबादी को छलते हैं। जब तक जाति-अन्त आन्दोलन इस व्यवहारवाद, सुधारवाद और अस्मितावाद के दलदल से निकलेगा नहीं, तब तक हमारे हालात में कोई बुनियादी सुधार नहीं हो सकता है।
तीसरी बात यह कि अय्यंकालि ने जाति अन्त के आन्दोलन को वर्ग संघर्ष से जोड़ दिया जब उन्होंने खेतिहर मज़दूरों की हड़ताल संगठित की और वह भी इसलिए ताकि सभी दलित बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। उन्होंने अपने संगठन को भी ग़रीब मेहनतकशों का संगठन बताया न कि किसी जाति-विशेष का। आज भी हमें इस बात को समझना होगा कि हम अगर दलित मुक्ति के संघर्ष में दलित जातिगत अस्मिता को आधार बनायेंगे, तो लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार जायेंगे। क्योंकि इसके ज़रिये हम ब्राह्मणवादी ताक़तों को यह मौक़ा देते हैं कि वे ग़ैर-दलित जातियों में भी अस्मितावाद को भड़काए। यदि सभी जातियाँ अपनी अस्मिताओं के आधार पर रूढ़ हो जायेंगी तो क्या हम जाति-अन्त की लड़ाई को जीत सकते हैं? कभी नहीं!
ब्राह्मणवादी पूँजीवादी शक्तियों को पराजित करने का रास्ता क्या है? यह कि हम ग़ैर-दलित जातियों के ग़रीब मेहनतकश लोगों को भी जाति-अन्त के आन्दोलन के साथ जोड़ दें और उन्हें दिखलाएँ कि उनके असली दुश्मन स्वयं उनकी जातियों के कुलीन और अमीर हैं, जो कि सारे संसाधनों पर कब्ज़ा जमाकर बैठे हैं। समस्त मेहनतकशों की वर्ग एकता के बूते ही दलित मेहनतकश आबादी मेहनतकशों के तौर पर अपने हक़ों को भी जीत सकती है और साथ ही जाति-अन्त के ज़रिये अपनी मुक्ति को हासिल कर सकती है। अस्मिताओं के टकराव में हम हमेशा हारेंगे। इसमें सभी ग़रीब मेहनतकश हारेंगे, चाहें वे किसी भी जाति के हों। इसलिए हमारे संघर्ष की ज़मीन अस्मितावाद और पहचान की राजनीति नहीं हो सकती, बल्कि ग़रीबों और मेहनतकशों की एक ऐसी राजनीति ही हो सकती है जो कि जाति-अन्त के प्रश्न को पुरज़ोर तरीक़े से उठाती हो। इसी वर्ग-आधारित साझे संघर्ष के ज़रिये ही तमाम ग़ैर-दलित जातियों के ग़रीब मेहनतकशों के जातिगत पूर्वाग्रहों को भी एक लम्बी प्रक्रिया में दोस्ताना संघर्ष से ख़त्म किया जा सकता है। ज़रा सोचिये साथियो! क्या आज तक अस्मिताओं के टकराव के रास्ते से समूची मेहनतकश आबादी के जातिगत पूर्वाग्रह ख़त्म हुए हैं, या बढ़े हैं? वे लगातार बढ़े हैं और इसका खामियाज़ा सबसे ज्यादा आम मेहनतकश दलित आबादी को और समूची मेहनतकश आबादी को उठाना पड़ा है। अय्यंकालि की विरासत हमें दिखलाती है कि सत्ता के ख़िलाफ़ आमूलगामी संघर्ष और जाति अन्त की लड़ाई में समूची मेहनतकश जनता को साथ लेकर ही हम जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ कारगर तरीक़े से लड़ सकते हैं।
साथियो! 18 जून को अय्यंकालि का स्मृति दिवस है। तमाम जाति-विरोधी व्यक्तित्वों को ख़ुद भारत की सरकार ने आज़ादी के बाद से ही प्रचारित-प्रसारित किया है लेकिन अय्यंकालि को नहीं। क्यों? क्योंकि अय्यंकालि आमूलगामी तरीक़े से और जुझारू तरीक़े से सड़क पर उतरकर संघर्ष का रास्ता अपनाते थे; क्योंकि अय्यंकालि सरकार की भलमनसाहत या समझदारी के भरोसे नहीं थे, बल्कि जनता की पहलक़दमी पर भरोसा करते थे। यही कारण है कि सरकार अय्यंकालि के जन्मदिवस या स्मृति दिवस पर कोई समारोह नहीं करती, कोई छुट्टी घोषित नहीं करती, उनकी तस्वीरें जगह-जगह नहीं लगाई जातीं और न ही उनकी प्रतिमाएँ खड़ी की जाती हैं। अय्यंकालि के रास्ते और विचारों के इस पक्ष को हमसे बचाकर रखती है। क्योंकि यदि मेहनतकश दलित और दमित जनता उनके बारे में जानेगी, तो उनके रास्ते के बारे में भी जानेगी और यह मौजूदा पूंजीवादी व जातिवादी सत्ता ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसके विरुद्ध रैडिकल संघर्ष के रास्ते को जनता जाने और अपनी पहलक़दमी में भरोसा पैदा करे। यही कारण है कि अय्यंकालि की विरासत को जनता की शक्तियों को याद करना चाहिए। उनकी स्मृतियों को प्रगतिशील ताक़तों को जीवित रखना चाहिए। उनके आन्दोलन के रास्ते को व्यापक मेहनतकश और दलित जनता में हमें ले जाना होगा।
इस पूरी जाति-अन्त की क्रान्तिकारी मुहिम में हमसे जुड़िये! हमसे सम्पर्क करिये!
जाति व्यवस्था का नाश हो!
ब्राह्मणवाद का नाश हो!
पूँजीवाद का नाश हो!
अय्यंकालि की विरासत जिन्दाबाद!
जाति-उन्मूलन का जुझारू संघर्ष जिन्दाबाद!
बिन हवा न पत्ता हिलता है!
बिन लड़े न कुछ भी मिलता है!
– दिशा छात्र संगठन